जब तक आदमी जिए जा रहा है
तब तक उघडते रिश्ते सिये जा रहा है।
सोज़े-रश्क की तपिश कम करने को
आदमी धुंआ पिए जा रहा है।
बेज़ा आरज़ुओं के कफ़स में आदमी
ज़ीस्त अपनी किए जा रहा है।
इक अनजाने डर का लबादा सदियों से
आदमी अदम तक लिए जा रहा है।
बढ़ती आबादी के बढ़ते आज़ार
बे-मतलब आदमी भीड़ में पीले जा रहा है।
"प्रताप" कब थमेगा ये सिलसिला नफ़रत का
समझदार भी अब नफ़रत में घिरे जा रहा है।
Subscribe to:
Post Comments (Atom)









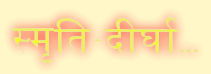






















No comments:
Post a Comment